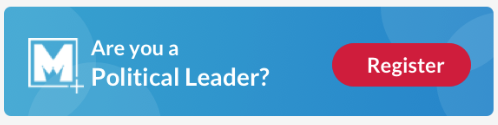कर्नाटक केस सिर्फ स्टेट पॉलिटिक्स नहीं, देश के विपक्ष की तस्वीर है!
कर्नाटक में जो कुछ हुआ है उसमें कोई नयी बात सामने आ रही है क्या? कर्नाटक भी विपक्ष की राष्ट्रीय राजनीति का आखिरी उत्पाद है जिसकी नींव मई, 2018 में बेंगलुरू में पड़ी थी. मौका था जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के शपथग्रहण का.
कर्नाटक में परदा गिरने के बाद जो कहानी सुनी जा रही है - वो बिलकुल वैसी ही है जो तस्वीर 2019 के आम चुनाव में देखने को मिली थी. विपक्षी एकता की एक तस्वीर 2015 के बिहार चुनाव में देखने को मिली थी, दूसरी तस्वीर कर्नाटक में कुमारस्वामी के शपथग्रहण के मौके पर और तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के कैराना उपचुनाव में - विपक्ष ने जैसा कर्म किया, फल भी उसे बिलकुल वैसा ही मिला है. दिल्ली से बेंगलुरू तक सूरत-ए-हाल बिलकुल एक ही है.
वैदिक काल में वनवास खत्म होने में 14 साल लग जाते हैं, लेकिन कर्म के प्रधान होने पर कलियुग में ये 14 महीने में भी भी खत्म हो सकता है - राजनीति के हर तिकड़म के महारत हासिल कर चुके बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में इसे साबित कर दिखाया है. येदियुरप्पा ने कर्नाटक में विपक्षी एकता को वैसे ही ध्वस्त कर डाला है जैसे आम चुनाव में मोदी-शाह की जोड़ी ने पूरे देश में.
14 महीने में विपक्षी एकता का वनवास
मई, 2018 में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का शपथग्रहण समारोह विपक्षी राजनीति के हिसाब से बड़ा मौका साबित हुआ. बेंगलुरू के उस आयोजन से पहले और उसके बाद कभी भी विपक्षी नेताओं की जमघट नहीं देखने को मिली.
सोनिया मायावती की हंसती-मुस्कुराती तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंचते ही वायरल हो गयीं - लगा जैसे 2019 के लोक सभा चुनाव में विपक्ष की जमघट ऐसी ही हुआ करेगी और नतीजे आने के बाद सभी यूं ही एक-दूसरे के गले मिलते नजर आएंगे. आगे वैसा कुछ भी नहीं हुआ.
कुछ होने को क्या कहा जाये ढाई दशक पुरानी दुश्मनी भुलाकर मायावती ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया और मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के साथ मंच शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के लिए वोट भी मांगा. यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फर्जी और मुलायम सिंह यादव को पिछड़ों का असली नेता तक बता डाला - लेकिन सोनिया गांधी की कांग्रेस को सपा-बसपा गठबंधन के आस पास फटकने तक नहीं दिया. गनीमत यही रही कि कांग्रेस के नाम पर अमेठी और रायबरेली की दो सीटें छोड़ दीं - लेकिन कांग्रेस सोनिया की सीट ही बचा पायी क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से हार गये.
कर्नाटक के इस जमावड़े के बाद यूपी के कैराना में उपचुनाव हुआ. गोरखपुर और फूलपुर चुनाव जीत चुके अखिलेश यादव और मायावती ने कैराना में भी हाथ मिलाये रखा - और नतीजा भी विपक्ष के ही पक्ष में आया. खास बात ये रही कि गोरखपुर और फूलपुर में उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दलों ने विपक्षी प्रत्याशी को ही सपोर्ट कर दिया था.
ऐसा लगा था कि कैराना उपचुनाव कर्नाटक में दिखी विपक्षी एकजुटता का पड़ाव होगा, लेकिन वो मंजिल ही साबित हुआ. विपक्षी नेताओँ ने मीटिंग तो खूब कीं, लेकिन बात कैराना से आगे नहीं बढ़ सकी. नतीजा ये हुआ कि बीजेपी पहले से भी ज्यादा सीटें जीत कर दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही.
विपक्षी एकता की डोर इतनी कमजोर क्यों?
विपक्षी एकजुटता की जितनी मजबूत डोर बेंगलुरू में नजर आयी थी वैसी न तो कोलकाता रैली, न पटना रैली और न ही दिल्ली रैली में कभी देखने को मिली. हर बार कोई न कोई नेता विपक्षी रैली से दूरी बना ले रहा था.
मायावती तो कर्नाटक में चुनावी गठबंधन के चलते भी मंच पर मौजूदगी दर्ज करा रही थीं, लेकिन उसके बाद न तो वो ममता बनर्जी की कोलकाता रैली में पहुंचीं, न ही अरविंद केजरीवाल द्वारा आयोजित दिल्ली की रामलीला मैदान रैली में. खैर, मायावती तो लालू प्रसाद की पटना रैली में भी नहीं पहुंची थीं. सोनिया गांधी और राहुल गांधी लालू की पटना रैली में पहुंचे तो नहीं थे, लेकिन संदेश जरूर भिजवाया था. वैसा ही रवैया कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैली को लेकर भी किया. दिल्ली में राहुल गांधी विपक्षी नेताओं से शरद पवार के घर पर तो मिले लेकिन रैली में झांकने तक नहीं गये. आखिर विपक्षी एकता की डोर इतनी कमजोर क्यों साबित होती है?
आम चुनाव के दौरान विपक्ष के मजबूत होने की कौन कहे, देश के कम ही हिस्से ऐसे रहे होंगे जहां दूसरे दलों के छोटे ही क्या बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन नहीं पकड़ा होगा. बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद तो जैसे विपक्षी दलों के नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने की रेस चल रही थी - और भगवा ओढ़ते ही सभी के जबान से एक ही बात निकलती - सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर वो अपनी पुरानी पार्टी के नेता के व्यवहार से बेहद दुखी हुए इसलिए राष्ट्रवाद की राजनीति का हिस्सा बनने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं.
ध्यान से देखिये तो जिस तरह दूसरे दलों से नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे थे, वही सिलसिला जारी है या कहें कि आगे बढ़ता जा रहा है. कर्नाटक में जो हुआ है वो वैसा ही है जैसा गोवा में हुआ है. तेलंगाना में हुआ है या आंध्र प्रदेश से आने वाले टीडीपी के राज्य सभा सांसदों ने कर दिखाया है. पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी के नेता भी तो वैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं.
राजनीतिक दृष्टि तो यही कह रही है कि कर्नाटक में बीजेपी की वापसी के लिए भी वही फैक्टर जिम्मेदार है जिसकी वजह से मोदी सरकार सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही - बिलकुल देश के सभी विपक्षी दल और उनके मतभेद या महत्वाकांक्षा. पूरे देश में विपक्षी दल लगातार आपस में लड़ते रहे और तमाम आलोचनाओं के बावजूद आम चुनाव में बीजेपी ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि प्रदर्शन में भी काफी सुधार कर लिया.
विश्वासमत में हार के बाद कुमारस्वामी जितना बीजेपी को बुरा भला कह रहे थे उतना ही खुद की किस्मत को भी कोस रहे थे. ऐसा भी तो नहीं कि कांग्रेस और जेडीएस को ये नुकसान अचानक हुआ है.
आम चुनाव में भी क्या हुआ राहुल गांधी ने तो सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के परिवारवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन कर्नाटक में भी तो वही चल रहा था. कमलनाथ जहां अपने बेटे को चुनाव जिताने में कामयाब रहे, वहीं अशोक गहलोत चूक गये. कर्नाटक में तो उससे भी बुरा हुआ कांग्रेस के बडे नेता मल्लिकार्जुन खड्गे तो बेटे के चक्कर में खुद ही चुनाव हार गये. हुआ ये कि मल्लिकार्जुन खड्गे के बेटे के चलते जिस कांग्रेस विधायक को कुमारस्वामी सरकार में जगह नहीं दी गयी - वो बीजेपी ज्वाइन कर मल्लिकार्जुन खड्गे से लड़ा और चारों खाने चित्त कर दिया.
विपक्षी नेताओं के तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कवायद बीते साल के आम चुनावों में भी देखी जाती रही है. पहले ये काम कभी मुलायम सिंह यादव तो कभी कोई और नेता किया करता रहा, इस बार एन. चंद्रबाबू नायडू और के. चंद्रशेखर राव के साथ साथ ममता बनर्जी, शरद पवार, एचडी देवगौड़ा जैसे नेता भी लगे रहे - लेकिन हर साल की तरह 2019 में भी वही हुआ - ढाक के तीन पात. कर्नाटक की कहानी भी उससे किसी भी मायने में अलग नहीं है.
कर्नाटक में परदा गिरने के बाद जो कहानी सुनी जा रही है - वो बिलकुल वैसी ही है जो तस्वीर 2019 के आम चुनाव में देखने को मिली थी. विपक्षी एकता की एक तस्वीर 2015 के बिहार चुनाव में देखने को मिली थी, दूसरी तस्वीर कर्नाटक में कुमारस्वामी के शपथग्रहण के मौके पर और तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के कैराना उपचुनाव में - विपक्ष ने जैसा कर्म किया, फल भी उसे बिलकुल वैसा ही मिला है. दिल्ली से बेंगलुरू तक सूरत-ए-हाल बिलकुल एक ही है.
वैदिक काल में वनवास खत्म होने में 14 साल लग जाते हैं, लेकिन कर्म के प्रधान होने पर कलियुग में ये 14 महीने में भी भी खत्म हो सकता है - राजनीति के हर तिकड़म के महारत हासिल कर चुके बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में इसे साबित कर दिखाया है. येदियुरप्पा ने कर्नाटक में विपक्षी एकता को वैसे ही ध्वस्त कर डाला है जैसे आम चुनाव में मोदी-शाह की जोड़ी ने पूरे देश में.
14 महीने में विपक्षी एकता का वनवास
मई, 2018 में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का शपथग्रहण समारोह विपक्षी राजनीति के हिसाब से बड़ा मौका साबित हुआ. बेंगलुरू के उस आयोजन से पहले और उसके बाद कभी भी विपक्षी नेताओं की जमघट नहीं देखने को मिली.
सोनिया मायावती की हंसती-मुस्कुराती तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंचते ही वायरल हो गयीं - लगा जैसे 2019 के लोक सभा चुनाव में विपक्ष की जमघट ऐसी ही हुआ करेगी और नतीजे आने के बाद सभी यूं ही एक-दूसरे के गले मिलते नजर आएंगे. आगे वैसा कुछ भी नहीं हुआ.
कुछ होने को क्या कहा जाये ढाई दशक पुरानी दुश्मनी भुलाकर मायावती ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया और मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के साथ मंच शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के लिए वोट भी मांगा. यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फर्जी और मुलायम सिंह यादव को पिछड़ों का असली नेता तक बता डाला - लेकिन सोनिया गांधी की कांग्रेस को सपा-बसपा गठबंधन के आस पास फटकने तक नहीं दिया. गनीमत यही रही कि कांग्रेस के नाम पर अमेठी और रायबरेली की दो सीटें छोड़ दीं - लेकिन कांग्रेस सोनिया की सीट ही बचा पायी क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से हार गये.
कर्नाटक के इस जमावड़े के बाद यूपी के कैराना में उपचुनाव हुआ. गोरखपुर और फूलपुर चुनाव जीत चुके अखिलेश यादव और मायावती ने कैराना में भी हाथ मिलाये रखा - और नतीजा भी विपक्ष के ही पक्ष में आया. खास बात ये रही कि गोरखपुर और फूलपुर में उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दलों ने विपक्षी प्रत्याशी को ही सपोर्ट कर दिया था.
ऐसा लगा था कि कैराना उपचुनाव कर्नाटक में दिखी विपक्षी एकजुटता का पड़ाव होगा, लेकिन वो मंजिल ही साबित हुआ. विपक्षी नेताओँ ने मीटिंग तो खूब कीं, लेकिन बात कैराना से आगे नहीं बढ़ सकी. नतीजा ये हुआ कि बीजेपी पहले से भी ज्यादा सीटें जीत कर दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही.
विपक्षी एकता की डोर इतनी कमजोर क्यों?
विपक्षी एकजुटता की जितनी मजबूत डोर बेंगलुरू में नजर आयी थी वैसी न तो कोलकाता रैली, न पटना रैली और न ही दिल्ली रैली में कभी देखने को मिली. हर बार कोई न कोई नेता विपक्षी रैली से दूरी बना ले रहा था.
मायावती तो कर्नाटक में चुनावी गठबंधन के चलते भी मंच पर मौजूदगी दर्ज करा रही थीं, लेकिन उसके बाद न तो वो ममता बनर्जी की कोलकाता रैली में पहुंचीं, न ही अरविंद केजरीवाल द्वारा आयोजित दिल्ली की रामलीला मैदान रैली में. खैर, मायावती तो लालू प्रसाद की पटना रैली में भी नहीं पहुंची थीं. सोनिया गांधी और राहुल गांधी लालू की पटना रैली में पहुंचे तो नहीं थे, लेकिन संदेश जरूर भिजवाया था. वैसा ही रवैया कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैली को लेकर भी किया. दिल्ली में राहुल गांधी विपक्षी नेताओं से शरद पवार के घर पर तो मिले लेकिन रैली में झांकने तक नहीं गये. आखिर विपक्षी एकता की डोर इतनी कमजोर क्यों साबित होती है?
आम चुनाव के दौरान विपक्ष के मजबूत होने की कौन कहे, देश के कम ही हिस्से ऐसे रहे होंगे जहां दूसरे दलों के छोटे ही क्या बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन नहीं पकड़ा होगा. बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद तो जैसे विपक्षी दलों के नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने की रेस चल रही थी - और भगवा ओढ़ते ही सभी के जबान से एक ही बात निकलती - सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर वो अपनी पुरानी पार्टी के नेता के व्यवहार से बेहद दुखी हुए इसलिए राष्ट्रवाद की राजनीति का हिस्सा बनने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं.
ध्यान से देखिये तो जिस तरह दूसरे दलों से नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे थे, वही सिलसिला जारी है या कहें कि आगे बढ़ता जा रहा है. कर्नाटक में जो हुआ है वो वैसा ही है जैसा गोवा में हुआ है. तेलंगाना में हुआ है या आंध्र प्रदेश से आने वाले टीडीपी के राज्य सभा सांसदों ने कर दिखाया है. पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी के नेता भी तो वैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं.
राजनीतिक दृष्टि तो यही कह रही है कि कर्नाटक में बीजेपी की वापसी के लिए भी वही फैक्टर जिम्मेदार है जिसकी वजह से मोदी सरकार सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही - बिलकुल देश के सभी विपक्षी दल और उनके मतभेद या महत्वाकांक्षा. पूरे देश में विपक्षी दल लगातार आपस में लड़ते रहे और तमाम आलोचनाओं के बावजूद आम चुनाव में बीजेपी ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि प्रदर्शन में भी काफी सुधार कर लिया.
विश्वासमत में हार के बाद कुमारस्वामी जितना बीजेपी को बुरा भला कह रहे थे उतना ही खुद की किस्मत को भी कोस रहे थे. ऐसा भी तो नहीं कि कांग्रेस और जेडीएस को ये नुकसान अचानक हुआ है.
आम चुनाव में भी क्या हुआ राहुल गांधी ने तो सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के परिवारवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन कर्नाटक में भी तो वही चल रहा था. कमलनाथ जहां अपने बेटे को चुनाव जिताने में कामयाब रहे, वहीं अशोक गहलोत चूक गये. कर्नाटक में तो उससे भी बुरा हुआ कांग्रेस के बडे नेता मल्लिकार्जुन खड्गे तो बेटे के चक्कर में खुद ही चुनाव हार गये. हुआ ये कि मल्लिकार्जुन खड्गे के बेटे के चलते जिस कांग्रेस विधायक को कुमारस्वामी सरकार में जगह नहीं दी गयी - वो बीजेपी ज्वाइन कर मल्लिकार्जुन खड्गे से लड़ा और चारों खाने चित्त कर दिया.
विपक्षी नेताओं के तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कवायद बीते साल के आम चुनावों में भी देखी जाती रही है. पहले ये काम कभी मुलायम सिंह यादव तो कभी कोई और नेता किया करता रहा, इस बार एन. चंद्रबाबू नायडू और के. चंद्रशेखर राव के साथ साथ ममता बनर्जी, शरद पवार, एचडी देवगौड़ा जैसे नेता भी लगे रहे - लेकिन हर साल की तरह 2019 में भी वही हुआ - ढाक के तीन पात. कर्नाटक की कहानी भी उससे किसी भी मायने में अलग नहीं है.
More videos
See AllRegister Login Articles Leaders Authors Caricatures Contact Us Privacy Policy Terms & Conditions
Follow Us - Facebook | Twitter | Youtube
Molitics © 2022